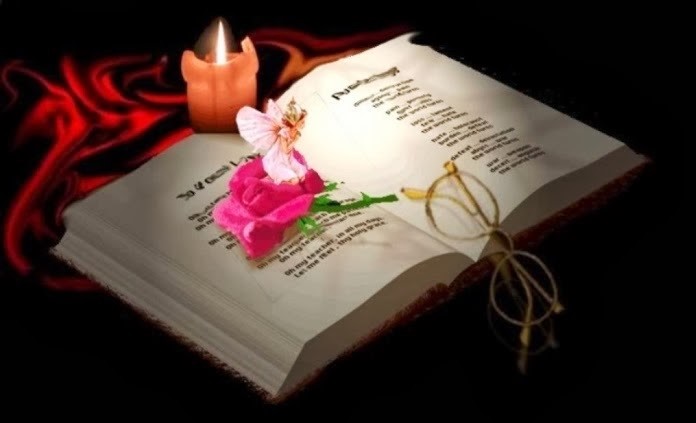अब गायें साँझ को
नहीं लौटतीं,
न ही उड़ाती हैं धूल
गोधूलि बेला में।
अब
सड़कों पर
नहीं दिखते गिल्ली- डण्डे
या गड्ढा-गेंद,
खेलते बच्चे
गायों के वन-वापसी की
प्रतीक्षा में।
बच्चे
पूर्व दिशा में उग आई
स्वयं से भी बड़ी
परछाईं
को दिखाने की अब नहीं
लगाते होड़,
और सूरज उदास हो
छुप जाता है
क्षितिज की गोद में,
अपनी सिन्दूरी में
सफेदी का बिना मिश्रण
लिए।
अब
चरवाहे
नहीं माँगते परितोषिक
गाभिन गाय की सुरक्षा
का,
न ही मनुहार करते हैं
वन में ब्यायी कबरी की
बछिया को,
सौंपते हुए गो-स्वामी
के हाथ,
जिसे पाँच कोस से
अपनी गोद में लेकर आ
रहा था वह।
अब
चरवाहों के हाथ में भी
नहीं है छाता,
कुल्हाड़ी और लाठी;
अब वे चाकरी की खोज
में
भटक रहे हैं
नगर-नगर,
गाँव-गाँव,
मालिकों के द्वार।
वनों
में घण्टियों के स्वर
अब विलुप्त हो चुके
हैं,
जो होती थीं
मार्गदर्शक
किसी भटके पथिक की।
वृक्ष,
जो देते थे
फूल-पत्ती और छाँव;
चट्टानें,
जिनमें मिलती थी
एक सूखी ठाँव;
नहरें,
जो बुझाती थीं प्यास,
देती थीं हरी-हरी घास—
और
मानव द्वारा
नृशंस हत्या किये जा
रहे वनों की आँखें
तरस रही हैं
अन्तिम गो-दर्शन को।
घरों से
खोते जा रहे हैं नाद
और चरी;
बाड़े तो जैसे अब
लुप्त ही हो चुके हैं,
जहाँ रात भर
छाँव में गो-समाज
करता था विश्राम
जुगाली के साथ।
खेतों में
ट्रैक्टरों का हो चुका है आधिपत्य,
और बैलों को कर दिया गया है मुक्त
उनके दायित्वों से।
कंक्रीट के घरों को
अब नहीं पड़ती
आवश्यकता
गोबर से लीपने की;
और उपलों–कण्डों
का विकल्प बन चुकी है
मीथेन।
दूध
मिल जाता है
दुग्धशाला में,
या थैलियों में बन्द
दुकानों में।
इसीलिए
देसी
गायों की उपयोगिता
पर खड़े हो चुके हैं
प्रश्नचिह्न कई—
क्योंकि वे होती हैं
कम दुधारू,
और संकरित गायों में
दुधैलता अधिक।
और
मनुष्य को
सबकुछ अधिक ही चाहिए;
वह घाटे का सौदा नहीं
करता,
क्योंकि जाति–धर्म से
चाहे वह कुछ भी हो,
पर विचार से
व्यापारी ही होता है।
अब तो
लाचार हैं गायें
अपनी उघड़ी–कँपकँपाती
देह पर ही
सहन करने को
भीषण मुसलाधार बारिश,
हाड़ सिकोड़ देने वाली
ठण्ड,
और
अग्निशिखाओं-युक्त
ताप-लहर भी।
असल में, गायें
कहीं जातीं ही नहीं।
लौटने के लिए जाना
आवश्यक होता है,
और उससे भी अधिक
आवश्यक होता है
एक ठौर का होना।
गाय
कामधेनु है,
गाय माता है,
परन्तु माता
अब निकेतन–हीन है।
मनुष्य की माँ के लिए
हैं—
कम-से-कम वृद्धाश्रम
बहुत;
परन्तु गो-माता
सड़कों पर
कुत्ते की मौत मर रही
है।
गायें,
माता होकर भी
खोज रही हैं
अस्तित्व अपना
घर-घर, द्वार–द्वार;
परन्तु मिल रही है
पुचकार के स्थान पर,
मात्र दुत्कार।
और गो-भक्त
गाय के पूत
मात्र वाहनों में
ले जायी जाती गायों
को ही मानते हैं माता,
और उसे छुड़ाने के लिए
रक्त–रंजित कर सकते
हैं किसी को भी।
बाकी
गायें
उनके लिए
पशु हैं, जानवर हैं—
जो कि ढोल, गँवार, शूद्र
और नारी की भाँति
ताड़ना की अधिकारी
हैं।
ऊसर–बंजर खेतों ने
छोड़ दिया है घास उगाना भी;
किसानों की खेती में
लग गये हैं
विद्युत्-युक्त बाड़े।
तालाबों से
निचोड़ लिया जाता है
जल सारा;
अतः
माएँ हैं लाचार—
खाने को कूड़ा–करकट,
और पीने को
गड्ढे का दूषित जल।
एक दिन गायों को भी
घोषित कर दिया जाएगा
‘आवारा’;
भेज दिया जाएगा
आश्रय-केन्द्रों में।
बैलों की कर दी जाएगी
नसबन्दी,
और रोक दिया जाएगा
उत्पत्ति
इस अनोखे जीव की।
गायें,
जो कि माता हैं,
जो कि हो चुकी हैं
उपेक्षित और आवासहीन—
अब कहीं नहीं जाएँगी,
न तो कहीं से आएँगी;
वे बस अपना आहार
चरने के दण्ड–स्वरूप
मार खाएँगी।
सम्भवतः
यह युग माओं को
अपमानित, आश्रयहीन और निराश्रित, निर्वासित
करने वाला ही है।