मैं उनकी ही ओर से आया हूँ—उनकी पीड़ा, उनकी खामोशियों और उनके अनकहे सन्देश
को लेकर। वे सिर्फ़ कह नहीं रहे—वे चीत्कार रहे हैं, बिलख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। सूखे हुए चेहरे और भूखी आँतें पुकार रही हैं—“आओ… देखो…
सुनो हमें।” हम भारत के लोग—भूख, प्यास, गरीबी और असमानता की करवटों में
तड़प रहे हैं। हम वही बच्चे हैं जो कल इस देश का भविष्य सँवारने वाले हैं, पर आज हमारा अपना भाग्य किसी अँधेरी खोह में दबा पड़ा है। जिस उम्र में हमारे
हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, वहाँ गाय की घण्टी और भैंस की
रस्सी पकड़ा दी गई है। जिस उम्र में हमारी अँगुलियाँ कलम थामकर काग़ज़ पर सपने
उकेरतीं, उसी उम्र में वे चकला–बेलन घुमा रही हैं, या दूसरों के घरों में झाड़ू–पोछा कर
रही हैं। जिस उम्र में हमें पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, उस उम्र में हम होटलों के जूठन
बटोरकर पेट भरने को मजबूर हैं।“
इतना ही नहीं, शासन की तमाम योजनाएँ होने के बावजूद भी हम आज भी अज्ञानता
के गहरे खोह में भटक रहे हैं। काग़ज़ों में पोषण की योजनाएँ चमकती हैं, पर हमारे गाँवों के सादे घरों में वे योजनाएँ कभी पहुँच ही
नहीं पातीं। आँगनबाड़ी के केन्द्र हैं, पर कितनी ही
माताएँ आज भी यह नहीं जानतीं कि उनके बच्चे को कब, क्या और कितना
खाना चाहिए। जागरूकता की कमी ने हमारे आहार को इतना कमजोर कर दिया है कि हमारे
शरीर पर मांस कम,
हड्डियों की गिनती
ज़्यादा दिखाई देती है। हमारे शरीर में उतना ही मांस है, जितने से कि हमारा सफ़ेद कंकाल
दिखाई न पड़े। कई बच्चों के पेट फूले हुए और शरीर सूखे तीलियों जैसे—यह सिर्फ़ भूख
नहीं, कुपोषण की चीख है।
गाँव की गलियों में घूमते
छोटे-छोटे बच्चे जब अपनी पतली टाँगों पर लड़खड़ाते दिखते हैं, तब लगता है जैसे पूरा गाँव उनके साथ लड़खड़ा रहा हो। किशोरियों
की स्थिति तो और भी भयावह है—रक्ताल्पता ने जैसे उनके जीवन का रंग ही चूस लिया हो।
हर महीने आने वाली कमजोरी, चक्कर, थकान… पर वे बोलती नहीं, क्योंकि उन्हें
लगता है—“कमजोरी तो लड़की होने का ही हिस्सा है।” अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केन्द्र भी हैं, पर दूरी, अज्ञानता और झिझक दीवारें बनकर खड़ी हैं। प्रसव के समय आज
भी कई घरों में दाई के भरोसे बच्चे जन्म लेते हैं, और कई बार—जच्चा
भी चली जाती है,
बच्चा भी। आँसुओं से भीगा
परिवार उस कमरे के बाहर खड़ा रह जाता है, जहाँ बस कुछ देर
पहले एक औरत जीवन देने की कोशिश कर रही थी। विद्यालय भी हैं, पर शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं। कक्षाओं में दीवारें हैं, कुर्सियाँ हैं, शिक्षक हैं—पर हम नहीं
हैं। क्योंकि हमें लगता है कि खेत अधिक ज़रूरी हैं, घर का काम अधिक
ज़रूरी है, पैसे अधिक ज़रूरी हैं। और इस सोच के कारण हमारे बच्चे आज भी
“पहली कक्षा से जीवन की कठिन परीक्षा” में सीधे धकेल दिए जाते हैं। गाँवों की यह
सच्चाई आँकड़ों में नहीं, इन थके चेहरों, इन सूखे पेटों, इन खाली विद्यालयों में
दिखाई देती है। यह दर्द केवल आँकड़े नहीं—जीते–जागते लोग हैं, जिनका भविष्य हर दिन थोड़ा-थोड़ा टूट रहा है। और हमारे साथ ये जो भी हो रहा है,
वह जानबूझकर नहीं हो रहा है, इसके पीछे अशिक्षा, अज्ञानता अजागरुकता बहुत बड़े कारण हैं।
मैं आज उन चीखों की आवाज़ बन कर आया हूँ, जो धूमिल हो चुके उन चेहरों के मौन चीखों का दर्पण है—जो हमारे गाँवों में, हमारे समाज में, हमारे ही बीच जीते हुए धीरे-धीरे मिटते जा रहे हैं। वे बहुत कुछ कह रहे हैं—इतना कि सुनने के लिए केवल हमारे कान पर्याप्त नहीं होंगे। हमें अपने मन, दिल, और मस्तिष्क—सबके द्वार खोलने होंगे। हमें अपनी इच्छा–शक्ति को जगाना होगा, अपने Logo के Ego से बाहर निकलना होगा, और अपनी सुविधाओं के खोल को त्याग कर उनकी जीवन-यात्रा में कदम रखना होगा। क्योंकि परिवर्तन दूर से खड़े होकर नहीं आता—परिवर्तन वहीं जन्म लेता है, जहाँ मनुष्य मनुष्य का हाथ थामता है। हमें उनके पास जाना होगा—उनके काँपते हाथ थामकर, उनकी आँखों में झाँककर, उनके हृदय की थरथराती आवाज़ सुनकर, उन्हें हिम्मत देते हुए यह कहना होगा—“हे भारत के लोग, हम भारत के लोग आपके अपने हैं… और आप हमारे। हम आपके बीच इसलिए आए हैं कि आपका दुःख समझ सकें, आपके संघर्ष को महसूस कर सकें, और आपके साथ मिलकर उन कष्टों का अन्त कर सकें। इस अभियान में हमारी नहीं—आपकी जीत छिपी है। क्या आप अपने भविष्य के लिए हमारा हाथ थामेंगे?”
साथियों, अब मैं उन भारत के लोगों की ओर से—उन बच्चों, किशोरियों, माताओं, खेतों में झुकते श्रमिकों की ओर
से— आपसे यह जानना चाहता हूँ—कि क्या आप तैयार हैं? इस देश का नागरिक होने के नाते, अपने के नागरिकों की आवाज़ सुनने, उनके साथ क़दम-से-क़दम मिलाकर चलने, और ज़िला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस मानवता–अभियान का हिस्सा बनने के लिए
तैयार हैं? “जब हम किसी एक जीवन को थामते हैं, हम पूरे समाज को उठाते हैं।” अब
निर्णय हम सबके हाथ में है—क्या हम आगे बढ़ेंगे?
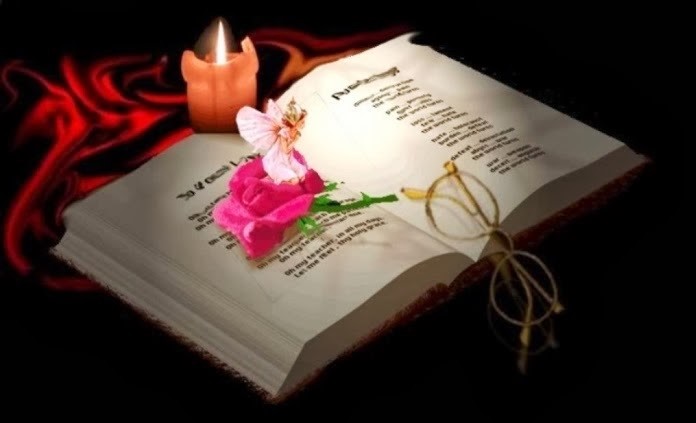

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें